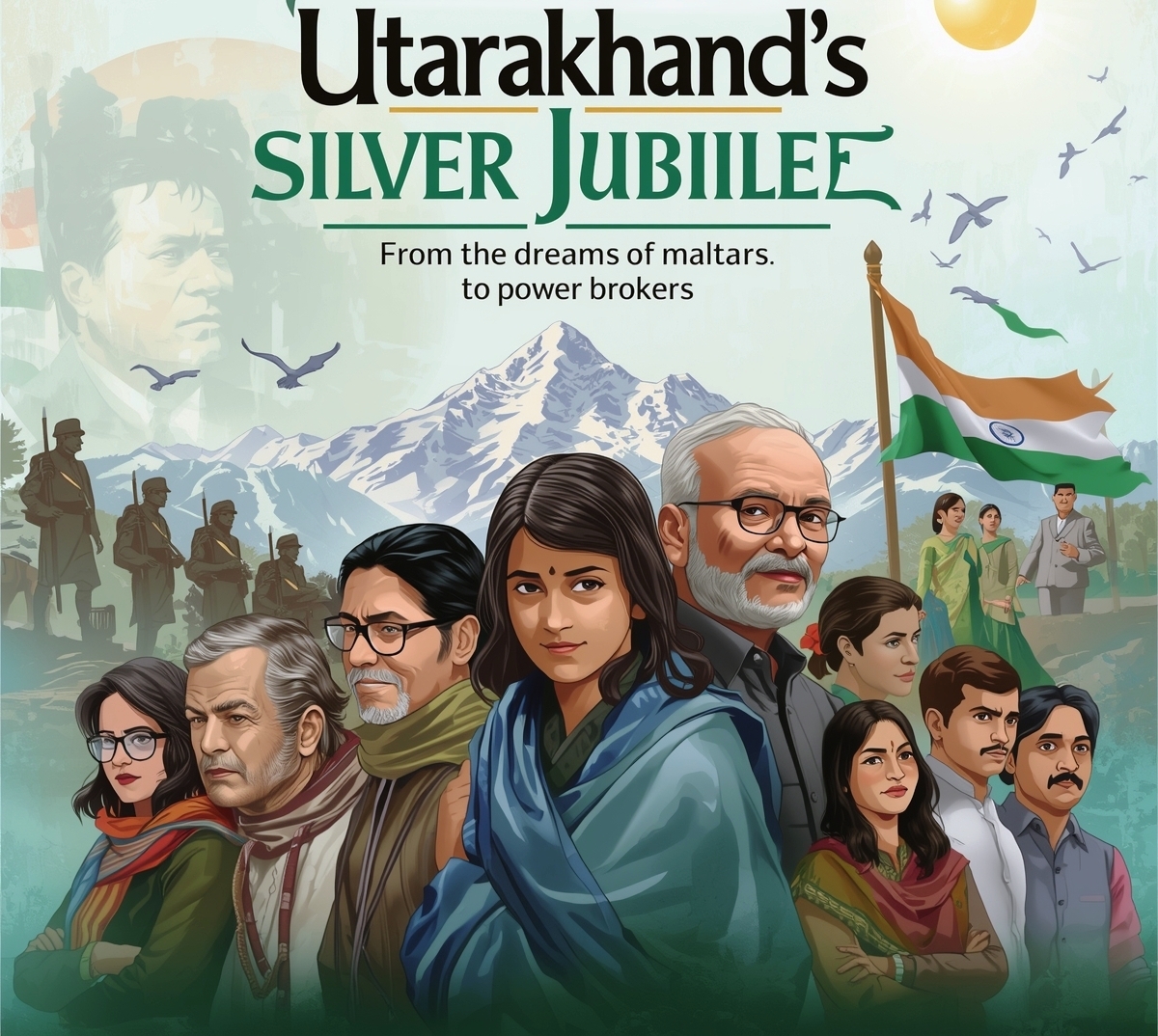उत्तराखंड की रजत जयंती: शहीदों के सपनों से सत्ता के सौदागरों तक — क्या यही था राज्य निर्माण का लक्ष्य?
25 वर्षों की यात्रा में उत्तराखंड — उपलब्धियों की गूंज के बीच जन-आकांक्षाओं की मौन चीख
उत्तराखंड की रजत जयंती की भूमिका और आंदोलन की आत्मा
केदार सिंह चौहान ‘प्रवर’
(सम्पादक, सरहद का साक्षी)
रजत जयंती के उजाले में सवालों की परछाइयाँ
उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर चुका है। यह क्षण औपचारिक रूप से उत्सव का प्रतीक है — लेकिन गहराई में झांकने पर यह उत्सव एक मौन प्रश्न भी है।
राज्य स्थापना की यह रजत जयंती हमें सिर्फ़ अतीत की उपलब्धियाँ नहीं, बल्कि अधूरे सपनों का आईना दिखा रही है।
सरकार और उसके विभाग अपनी-अपनी सफलताओं का प्रचार कर रहे हैं — योजनाओं की सूची, निर्माण कार्यों की गिनती, पर्वतीय पर्यटन की चमक, और निवेश के दावे।
परंतु इस आडंबर के पीछे एक सच्चाई छिपी है — पर्वतीय जनता की जमीनी हकीकत, जो अब भी उस राज्य की खोज में है जिसका सपना उसने 1990 के दशक में देखा था।
1994 की देहरादून, मुजफ्फरनगर, रामपुर तिराहा, खटीमा, मसूरी की गलियों में जो नारे गूंजे थे —
“अपना राज्य—अपना शासन”,
“जय उत्तराखंड मातृभूमि”,
“अब दिल्ली नहीं, देहरादून चलेगा शासन” —
वो सिर्फ़ नारों की गूंज नहीं थी, वह आत्मसम्मान की पुकार थी।
पर आज, 25 वर्षों बाद, जब राज्य अपनी रजत जयंती के मुकाम पर है, यह सवाल खुद खड़ा है —
“क्या वह स्वराज्य, वह स्वाभिमान, और वह संवेदना अब भी जीवित है?”
उत्तराखंड राज्य निर्माण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की नींव दशकों पुरानी थी।
ब्रिटिश काल से ही यह भू-भाग — गढ़वाल, कुमाऊँ और जौनसार-बाबर — अलग प्रशासनिक समस्याओं से जूझता रहा।
1948 में गढ़वाल-कुमाऊँ का संयुक्त उत्तर प्रदेश में विलय, उस समय व्यावहारिक लग सकता था, लेकिन भूगोल, संस्कृति और सामाजिक ढांचे में अंतर ने हमेशा इस क्षेत्र को ‘हाशिए का हिस्सा’ बना दिया।
“पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी — कभी पहाड़ के काम नहीं आती” —
यह कहावत उत्तराखंड की नियति बन गई थी।
1980 के दशक में उत्तर प्रदेश सरकारों की नीतियों ने इस असमानता को और गहरा किया।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और सिंचाई — हर क्षेत्र में उपेक्षा बढ़ती गई।
नौजवानों में आक्रोश था, महिलाओं में असंतोष था, और समाज में परिवर्तन की मांग थी।
यहीं से प्रारंभ हुआ उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन।
“वंदे मातरम्” से “जय उत्तराखंड” तक — जनांदोलन की आत्मा
1994 का रामपुर तिराहा कांड इस आंदोलन की चिंगारी को ज्वाला में बदल गया।
मुजफ्फरनगर की उस स्याह रात में जब निर्दोष महिलाओं पर गोलियां चलीं,
तो यह सिर्फ़ जनसंहार नहीं था — यह उस अवमानना की पराकाष्ठा थी जिसे पहाड़ ने वर्षों झेला था।
उसके बाद आंदोलन गाँव-गाँव, घर-घर फैल गया।
पहाड़ की माताएं, बहनें, छात्र, शिक्षक, और बेरोजगार युवा — सब एक स्वर में बोल उठे,
“हमें अपना राज्य चाहिए — जहाँ हम अपने सपनों का शासन बना सकें।”
यह आंदोलन किसी दल का नहीं था, यह जनभावना की क्रांति थी।
इसमें न सत्ता का आकर्षण था, न पद का लोभ — यह था अपने अस्तित्व की लड़ाई।
शहीदों के सपने: आत्मनिर्भर, पारदर्शी और संवेदनशील राज्य
जब आंदोलन की अग्नि में राज्य का स्वप्न गढ़ा गया, तब उस स्वप्न की तीन प्रमुख धुरियाँ थीं —
आर्थिक स्वावलंबन:
पहाड़ की खेती, फलोद्यान, जड़ी-बूटी, जल-संसाधन और पर्यटन पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था।
प्रशासनिक पारदर्शिता:
एक ऐसा शासन-तंत्र जो दिल्ली पर निर्भर न रहे, बल्कि जनता की चौपाल से दिशा पाए।
सामाजिक समानता:
महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण युवाओं के अवसर, और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की गारंटी।
इन आदर्शों के लिए 300 से अधिक आंदोलनकारियों ने अपने प्राण न्योछावर किए।
उनकी आत्मा ने यह कहा था —
“हमारा राज्य ऐसा हो जहाँ कोई युवा बेरोजगार न रहे, कोई गांव वीरान न हो, कोई माँ अपने बेटे को दिल्ली पलायन में खो न दे।”
सत्ता बनाम संवेदना — आज का यथार्थ
लेकिन आज जब हम रजत जयंती मना रहे हैं, तो यह प्रश्न अनिवार्य है —
क्या वह सपना साकार हुआ?
सत्ता की गलियों में आंदोलन की संवेदनाएं खो चुकी हैं।
“राज्य आंदोलनकारी” शब्द अब राजनीतिक उपाधि बन गया है।
जो लोग आंदोलन में अग्रणी थे, वे भुला दिए गए;
और जिन्होंने सिर्फ़ पोस्टर लगाए, वे आज पेंशन, सम्मान और सुविधा के पात्र बन बैठे हैं।
पत्रकार जिन्होंने अपनी कलम से आंदोलन की मशाल जलाए रखी —
वे किसी सूची में शामिल नहीं, क्योंकि सत्य लिखना सत्ता को असहज करता है।
यह राजनीतिक निष्ठुरता उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी है।
विभागीय उपलब्धियों की चमक — और जनता की सिसकियाँ
रजत जयंती वर्ष के अवसर पर जब विभाग विशेषांक निकाल रहे हैं —
तो वे अपने आंकड़ों में सफलता के शिखर दिखाते हैं।
लेकिन जब वही विभाग जनता की अदालत में उतरते हैं,
तो सवाल उठते हैं —
क्या शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है?
क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर हैं?
क्या सड़कों ने गाँवों को जोड़ा है या सिर्फ़ फाइलों में नक्शे बने हैं?
क्या रोजगार योजनाएं कागजों से आगे बढ़ पाई हैं?
इन प्रश्नों के उत्तर आज भी “न” में हैं।
"जीरो टॉलरेंस" बनाम "कमीशन कल्चर"
उत्तराखंड की सरकारें एक नारे के साथ चलती आई हैं — “भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस।”
परंतु हाल के वर्षों में जब यह उजागर हुआ कि विधायकों के वेतन तक में कमीशनखोरी होती है,
तो यह नारा उपहास बन गया।
जनप्रतिनिधि यदि अपनी तनख्वाह में भी पारदर्शिता नहीं रख सकते,
तो जनता की योजनाओं में ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जाए?
यह स्थिति चिंतनीय ही नहीं — राज्य की आत्मा पर चोट है।
आंदोलन की आत्मा से संवाद : एक आह्वान
राज्य निर्माण आंदोलन सिर्फ़ राजनीतिक संघर्ष नहीं था — यह आध्यात्मिक क्रांति थी।
इसमें संस्कृति, प्रकृति और समाज का संगम था।
यह पहाड़ के जीवन-मूल्यों का आंदोलन था —
जहाँ त्याग, सेवा और सामूहिकता सर्वोपरि थी।
आज आवश्यकता है कि हम पुनः उसी आत्मा से जुड़ें।
राज्य का भविष्य तभी सुरक्षित है जब हम उस मूल भाव को पुनः जगा सकें —
“उत्तराखंड किसी दल का नहीं, जनमानस का राज्य है।”
विकास की चमक में छिपे अंधेरे — योजनाओं के आँकड़े बनाम जनता की पीड़ा
विभागीय रिपोर्ट कार्ड बनाम जमीनी हकीकत
रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य के विभिन्न विभागों ने अपनी-अपनी “विकास पुस्तिकाएँ” प्रकाशित की हैं — जिनमें सड़क निर्माण, शिक्षा सुधार, जल संरक्षण, पर्यटन विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाएँ, महिला सशक्तिकरण, और कृषि संवर्द्धन जैसी योजनाओं की लंबी सूची दी गई है।
लेकिन जब हम इन रिपोर्टों के पीछे छिपी वास्तविकता की परतें खोलते हैं, तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है।
सड़कें बनी हैं — पर ढलानों के नीचे गाँव खाली हो गए हैं।
पेयजल योजनाओं के उद्घाटन हुए — पर आज भी पहाड़ की महिलाएं सिर पर घड़ा रखे तीन किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं।
स्कूलों की इमारतें खड़ी हैं — पर शिक्षक अनुपस्थित हैं, छात्र पलायन कर चुके हैं।
स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी — पर डॉक्टरों की संख्या घट गई।
यह वही स्थिति है, जिसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने कभी लिखा था —
“उत्तराखंड में विकास का अर्थ आँकड़ों का विस्तार है, संवेदना का नहीं।”
स्वास्थ्य सेवाएँ — राज्य की सबसे बड़ी विफलता
राज्य आंदोलन के दौरान यह घोषणा हुई थी कि “प्रत्येक गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक अस्पताल” होगा।
लेकिन रजत जयंती के समय यह वादा सबसे अधिक अधूरा साबित हुआ है।
वास्तविकता के आंकड़े (2024 तक)
राज्य के 13 जिलों में कुल 1350 स्वास्थ्य उपकेंद्र दर्ज हैं,
परंतु इनमें से 40% से अधिक बिना डॉक्टर या नर्स के हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में 30% केंद्र सालभर दवाइयों के अभाव में बंद रहते हैं।
जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिक्ति दर 55% से अधिक है।
सर्वाधिक विडंबना यह है कि राजधानी देहरादून में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में प्रसूति या आपातकालीन सेवाएं भी समय पर नहीं मिलतीं।
“जहाँ सड़क खत्म होती है, वहाँ जीवन भी प्रशासन की पहुँच से बाहर हो जाता है।”
चंबा जनस्वास्थ्य सत्याग्रह – एक प्रतीकात्मक चेतावनी
हाल ही में टिहरी जनपद के चंबा में “जन स्वास्थ्य सत्याग्रह” आंदोलन ने यह स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली केवल आंकड़ा नहीं, जनजीवन की त्रासदी बन चुकी है।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और ग्रामीण जब सर्द रातों में धरने पर बैठे रहे, तो यह केवल अस्पताल की मांग नहीं थी —
यह उस व्यवस्था के खिलाफ पुकार थी जिसने जनता की पीड़ा को फाइलों में दफना दिया।
शिक्षा — ज्ञान का दीप या बेरोजगारी की लौ?
उत्तराखंड कभी “शिक्षित राज्य” कहलाता था।
गढ़वाल और कुमाऊँ की धरती ने देश को असंख्य शिक्षक, अधिकारी, वैज्ञानिक, लेखक और सैनिक दिए।
लेकिन पिछले दशक में शिक्षा का स्तर बुरी तरह गिरा है।
वर्तमान स्थिति (2025 तक)
राज्य में 13 हजार से अधिक विद्यालय हैं,
परंतु 8000 से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं।
एनसीएफ-2020 के लागू होने के बावजूद शिक्षण सामग्री और डिजिटल संसाधनों की भारी कमी है।
पर्वतीय विद्यालयों में छात्र संख्या लगातार घट रही है, क्योंकि माता-पिता पलायन कर रहे हैं।
उच्च शिक्षा में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है।
शिक्षा अब रोजगार की गारंटी नहीं, बल्कि प्रवासन की तैयारी बन गई है।
पर्वतीय परिवार अपने बच्चों को देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली भेज रहे हैं —
क्योंकि गाँवों में शिक्षा का मतलब अब सिर्फ़ नाममात्र की उपस्थिति है।
“जहाँ शिक्षक नहीं, वहाँ भविष्य नहीं;
और जहाँ भविष्य नहीं, वहाँ राज्य केवल नक्शे पर रह जाता है।”
रोजगार और पलायन — राज्य की आत्मा का क्षरण
राज्य आंदोलन का सबसे बड़ा नारा था — “रोजगार हमारा अधिकार है।”
परंतु 25 वर्षों में यह अधिकार सबसे अधिक उपेक्षित रहा।
पलायन आयोग की रिपोर्ट (2023)
राज्य के 6,300 गाँवों में से 1,800 गाँव पूर्णतः खाली हो चुके हैं।
2.5 लाख से अधिक युवा स्थायी रूप से मैदानों और मेट्रो शहरों में बस चुके हैं।
1994–2025 के बीच राज्य से औसतन 20 लाख लोगों ने अस्थायी या स्थायी रूप से पलायन किया।
पलायन का यह प्रवाह केवल रोजगार की कमी नहीं, बल्कि राज्य व्यवस्था की विफलता का परिणाम है।
जब एक माँ अपने बेटे को सेना में भर्ती कराने के लिए दिल्ली भेजती है,
तो वह केवल नौकरी नहीं — अपने पहाड़ के सपने को मैदानों में बेचती है।
सरकारी रोजगार बनाम अनुबंध संस्कृति
सरकारी विभागों में स्थायी नियुक्तियों की जगह आउटसोर्सिंग और ठेके पर कार्य व्यवस्था ने युवा वर्ग को अस्थिर बना दिया है।
आज शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, चालक — सब ठेके पर हैं।
उनके अधिकार सीमित हैं, पर दायित्व अनंत।
“राज्य जहाँ कर्मचारी अस्थायी हों, वहाँ नीतियाँ भी अस्थायी हो जाती हैं।”
ठेकेदारी व्यवस्था — विकास का ‘दलाली मॉडल’
उत्तराखंड में विकास का सबसे चर्चित शब्द बन चुका है — “टेंडर”।
सड़क, भवन, पेयजल, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य — हर क्षेत्र में अब ठेकेदार ही नीति-निर्माता बन चुके हैं।
सरकारें बदलती हैं, लेकिन ठेकेदारों का नेटवर्क वही रहता है।
बोली से पहले ‘समझौता’, और काम के बाद ‘कमीशन’ — यही विकास का नया फार्मूला है।
परिणाम:
सड़कें बारिश में धस जाती हैं, क्योंकि गुणवत्ता गिरवी रखी जाती है।
जल योजनाएं सालभर में सूख जाती हैं, क्योंकि पाइप घटिया होते हैं।
विद्यालय भवन अधूरे रहते हैं, क्योंकि भुगतान पहले ही हो चुका होता है।
यह ठेकेदार संस्कृति अब राज्य के सामाजिक ढांचे में जहर की तरह फैल चुकी है।
सच्चे इंजीनियर, ईमानदार अधिकारी, और जिम्मेदार पंचायतें — सब हाशिए पर हैं।
“जब नीति ठेके में और नीयत कमीशन में बदल जाए,
तब विकास केवल उद्घाटन समारोह बन जाता है।”
महिला शक्ति — आंदोलन की रीढ़, पर नीति से बाहर
उत्तराखंड आंदोलन की आत्मा थीं पहाड़ की महिलाएँ।
चिपको से लेकर राज्य निर्माण तक, उन्होंने अपने आँचल से क्रांति को ढका।
लेकिन आज, वही महिला नीति-निर्माण में सबसे कम प्रतिनिधित्व रखती है।
सत्य यह है:
ग्राम पंचायतों में 50% आरक्षण के बावजूद निर्णय पुरुष प्रतिनिधि ही लेते हैं।
महिला स्वसहायता समूह (SHG) योजनाएँ अब कागजी उद्यम बन गई हैं।
पर्वतीय महिला आज भी लकड़ी, पानी और घास के लिए वही संघर्ष कर रही है जो उसकी दादी ने किया था।
राज्य में “महिला सशक्तिकरण विभाग” जरूर है, पर उसका फोकस सेमिनार और पोस्टर तक सीमित है।
महिला उद्यमिता, स्वरोजगार और स्वास्थ्य सुधार पर व्यावहारिक नीति नहीं बन पाई।
“जिस स्त्री ने राज्य बनाया, वह राज्य की योजना में नहीं — फोटो फ्रेम में रह गई।”
पर्यावरण और आपदाएँ — प्रकृति की चेतावनी
उत्तराखंड का भूगोल प्रकृति की गोद है — पर यह गोद अब कराहने लगी है।
बेतहाशा निर्माण, अनियंत्रित खनन, और नदियों के दोहन ने राज्य को आपदा प्रदेश बना दिया है।
2013 की केदारनाथ त्रासदी ने जो चेतावनी दी थी,
वह 2025 तक आते-आते नियोजनहीन विकास की कहानी बन गई है।
जमीन खिसक रही है, जलवायु बदल रही है, और गाड़-गदेरे अब नालों में बदल चुके हैं।
जो राज्य “जलविद्युत संपदा” से भरपूर था, वह अब बिजली की खरीद में करोड़ों खर्च कर रहा है।
“जब विकास प्रकृति की मर्यादा लाँघ जाए,
तो विनाश उसका उत्तर बनता है।”
पर्यावरणीय असंतुलन ने न केवल पहाड़ की मिट्टी को कमजोर किया,
बल्कि समाज की नींव — कृषि और पशुपालन — को भी समाप्त कर दिया।
रजत जयंती का दर्पण
रजत जयंती केवल जश्न का अवसर नहीं — आत्ममंथन का अवसर है।
राज्य की उपलब्धियाँ यदि सचमुच जनता तक पहुँचतीं,
तो चंबा, पोखरी, कपकोट, धारचूला, और मोरी जैसे कस्बों में आज भी धरने नहीं लगते।
25 वर्षों की यात्रा में जो हासिल हुआ, उसे नकारा नहीं जा सकता —
पर जो खोया गया, वह कहीं अधिक मूल्यवान है —
जनविश्वास, पारदर्शिता, और संवेदना।
“राज्य तब सफल नहीं होता जब उसके मंत्री समृद्ध हों,
बल्कि तब होता है जब उसकी जनता संतुष्ट हो।”
भविष्य की दिशा – पुनर्जागरण का समय, पुनर्विचार की आवश्यकता
उत्तराखंड 2040 की कल्पना — एक संवेदनशील, स्वावलंबी और सांस्कृतिक राज्य
रजत जयंती के अवसर पर हमें केवल बीते 25 वर्षों का लेखा-जोखा नहीं देखना चाहिए,
बल्कि आने वाले 25 वर्षों का स्वप्न भी गढ़ना चाहिए।
2025 से 2040 तक की यह यात्रा तय करेगी कि उत्तराखंड केवल “देवभूमि” कहलाएगा, या “विकासभूमि” भी बनेगा।
आज जब देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है,
तो उत्तराखंड को चाहिए कि वह अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करे —
आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नैतिक प्रशासन के तीन स्तंभों पर।
आत्मनिर्भर उत्तराखंड — संसाधनों पर जनता का अधिकार
राज्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि यहाँ की प्राकृतिक संपदा पर बाहरी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ता गया।
हाइड्रो प्रोजेक्ट हों या खनन क्षेत्र —
स्थानीय लोगों को केवल श्रमिक बनाया गया, स्वामित्व नहीं दिया गया।
यदि वास्तव में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना है,
तो निम्न पाँच सुधार प्राथमिकता बनने चाहिए —
1️⃣ जल-ऊर्जा पर स्थानीय स्वामित्व
राज्य के 50% से अधिक जलविद्युत प्रोजेक्ट बाहरी कंपनियों द्वारा संचालित हैं।
हर ब्लॉक में मिनी माइक्रो हाइड्रो प्लांट स्थापित कर,
ग्राम पंचायतों को ‘ऊर्जा सहकारी समितियों’ के रूप में स्वामित्व दिया जाए।
जिससे राजस्व भी गाँव में रहे और बिजली भी आत्मनिर्भर बने।
2️⃣ जैविक खेती का राज्यव्यापी मॉडल
उत्तराखंड के पास हिमालयी मिट्टी, जलवायु और प्राकृतिक उर्वरता है —
परंतु रासायनिक खेती ने इस सौंदर्य को नष्ट कर दिया।
यदि हर ब्लॉक में जैविक उत्पाद मंडी, शीतगृह और प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाए,
तो पलायन को रोका जा सकता है।
आज सच्ची चुनौती खेती में “ब्रांड वैल्यू” जोड़ने की है।
“जब गाँव की मिट्टी बाजार में अपनी पहचान पाएगी, तब पहाड़ की पीड़ा घटेगी।”
3️⃣ स्थानीय उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ना
मंडवा, झंगोरा, गहत, भट्ट, और बुरांश जैसे उत्पाद केवल स्मृति न रहें —
इनकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए राज्य को ‘हिमालय ब्रांड पोर्टल’ बनाना होगा।
यह “मेक इन उत्तराखंड” की सच्ची परिभाषा होगी।
4️⃣ पर्यटन का संतुलित विस्तार
उत्तराखंड के पहाड़ केवल तीर्थ नहीं, संवेदनशील पारिस्थितिकी भी हैं।
“कैरीइंग कैपेसिटी आधारित पर्यटन नीति” (Carrying Capacity Based Policy)
अपनाए बिना पर्वतीय क्षेत्र ओवर-टूरिज्म से टूट जाएंगे।
ग्राम पर्यटन, होमस्टे, वॉकिंग ट्रेल्स और स्थानीय संस्कृति को केंद्र में लाकर
“देवभूमि” को “संस्कृति-पर्यटन राज्य” के रूप में विकसित किया जा सकता है।
5️⃣ युवाओं के लिए उद्यमिता नीति
राज्य का भविष्य युवाओं में है।
हर वर्ष लगभग 2.5 लाख युवा बेरोजगार हो रहे हैं।
यदि हर जिले में स्टार्टअप फंड, स्किल सेंटर और मेंटर नेटवर्क बने,
तो पहाड़ के युवा खुद रोजगारदाता बन सकते हैं।
“युवा जब अपने गाँव में रहकर उद्यम करेगा, तभी राज्य जीवित रहेगा।”
सांस्कृतिक पुनर्जागरण — लोक परंपरा ही पहचान है
उत्तराखंड की सबसे बड़ी पूंजी उसकी संस्कृति और लोक चेतना है।
लेकिन पिछले वर्षों में यह पूंजी हाशिए पर चली गई।
गीत, नृत्य, बोली, पोशाक, तीज-त्योहार — सब धीरे-धीरे शहरीकरण के दबाव में खो रहे हैं।
संस्कृति को नीति से जोड़ना होगा
विद्यालय स्तर पर गढ़वाली-कुमाऊँनी लोकसाहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
“राज्य लोककला अकादमी” को पुनर्जीवित कर,
कलाकारों को नियमित आर्थिक सहयोग दिया जाए।
गाँव-गाँव में संस्कृति ग्राम परिषदें बनें, जो लोकगीत, नृत्य और परंपरा को पुनर्जीवित करें।
“उत्तराखंड दिवस” केवल सरकारी भाषण न हो —
बल्कि प्रत्येक ब्लॉक में “जन भागीदारी सांस्कृतिक महोत्सव” बने।
“संस्कृति ही वह धागा है, जो राज्य को राजनीति से ऊपर जोड़ता है।”
लोकभाषा की पुनर्स्थापना
भाषा केवल संवाद नहीं, पहचान है।
गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी भाषाओं के संरक्षण के लिए
“राज्य भाषा आयोग” को वास्तविक अधिकार दिए जाएँ।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानीय कंटेंट तैयार करना और उसे
राष्ट्रीय मीडिया तक पहुँचाना आवश्यक है।
शासन सुधार — पारदर्शिता से ही विश्वास लौटेगा
आज राज्य में सबसे बड़ा संकट विश्वास का संकट है।
सरकार की नीतियों और जनता के अनुभवों में गहरी खाई है।
इसे पाटने के लिए शासन व्यवस्था में निम्न सुधार अनिवार्य हैं —
1. स्थानीय जवाबदेही तंत्र
हर विकासखंड में “जन-निगरानी समिति” (Citizen Audit Group) बनाई जाए
जो हर छह माह में सरकारी योजनाओं की स्थिति का सार्वजनिक ऑडिट करे।
इससे न केवल भ्रष्टाचार घटेगा, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
2. ठेकेदारी व्यवस्था पर नियंत्रण
राज्य की निर्माण नीतियों में “कमीशन कल्चर” को समाप्त करने के लिए
“ई-टेंडरिंग की स्वतंत्र समीक्षा” और “कार्य गुणवत्ता मूल्यांकन आयोग” बनाया जाए।
काम पूरा होने के बाद 6 माह तक भुगतान रोककर गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए।
3. वित्तीय अनुशासन और वेतन पारदर्शिता
विधायकों व मंत्रियों के वेतन में कटौती कर उसे
“शहीद आंदोलनकारी कल्याण कोष” में दिया जाए।
जब जनता बलिदान देती है, तो शासक वर्ग को भी त्याग दिखाना होगा।
4. जनता से संवाद की संस्कृति
हर जनपद में माह में एक दिन “जन-संवाद दिवस” अनिवार्य किया जाए
जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, विधायक, पत्रकार और जनप्रतिनिधि एक साथ बैठें।
जनता की शिकायतें यहीं निपटाई जाएँ।
यह लोकतंत्र को प्रशासन से जोड़ने का माध्यम बनेगा।
“सत्ता जब जनता से संवाद खो देती है, तब जनता आंदोलन की भाषा में बोलती है।”
पर्यावरणीय पुनर्संतुलन — विकास और प्रकृति का संवाद
उत्तराखंड की आत्मा उसके पहाड़, नदियाँ और जंगल हैं।
परंतु यह आत्मा आज विकास के बोझ तले दब गई है।
विकास की परिभाषा को बदलना होगा — सतत विकास (Sustainable Development) के रूप में।
नीति सुधार के तीन सूत्र
1️⃣ पर्यावरणीय प्रभाव का स्थानीय मूल्यांकन (LEIA):
हर परियोजना का मूल्यांकन केवल देहरादून या दिल्ली के विशेषज्ञ नहीं करें —
बल्कि स्थानीय नागरिक समिति करे, क्योंकि वही जानते हैं कि पहाड़ किस बोझ को सह सकता है।
2️⃣ ‘एक नदी, एक समिति’ मॉडल:
गंगा, यमुना, काली, और गोरी जैसी नदियों के लिए
स्थानीय ग्राम पंचायतों, NGO और प्रशासन की संयुक्त नदी परिषदें बनाई जाएँ।
3️⃣ ‘ग्रीन बजट नीति’:
हर विभाग के बजट का कम से कम 10% पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आरक्षित हो।
यदि सड़क बने तो साथ में वृक्षारोपण और जलस्रोत पुनर्जीवन अनिवार्य हो।
“पहाड़ केवल पत्थर नहीं, जीवित परंपरा हैं;
इन्हें बचाना विकास नहीं, अस्तित्व की रक्षा है।”
युवाशक्ति — आंदोलन की अगली पीढ़ी
उत्तराखंड के युवा केवल रोजगार नहीं चाहते, भूमिका चाहते हैं।
वे राजनीति, नीति और नेतृत्व में स्थान चाहते हैं।
राज्य निर्माण की भावना को नया नेतृत्व चाहिए
विश्वविद्यालयों में ‘राज्य चेतना पाठ्यक्रम’ लागू किया जाए,
ताकि नई पीढ़ी को राज्य आंदोलन का इतिहास समझ में आए।
पंचायत चुनावों में 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व आरक्षित किया जाए।
युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘पर्वतीय स्टार्टअप मिशन’ शुरू किया जाए।
राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए न्यायिक आयोग पुनः गठित किया जाए
ताकि असली योगदानकर्ताओं को सम्मान और अवसर दोनों मिले।
“जो पीढ़ी अपने इतिहास को नहीं जानती, वह अपने भविष्य की रक्षा नहीं कर सकती।”
मीडिया और समाज — संवाद का पुनर्निर्माण
मीडिया का दायित्व केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज को जाग्रत करना भी है।
उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में मीडिया का चरित्र
लोकशक्ति और सरकार के बीच सेतु का होना चाहिए।
सरकारों को चाहिए कि स्थानीय डिजिटल मीडिया, जनपत्रकारिता और जनसंचार संस्थानों को सहयोग दें,
क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पहाड़ की आवाज़ राष्ट्रीय विमर्श तक पहुँचती है।
“मीडिया जब सत्ता का दर्पण नहीं, समाज का दीपक बने —
तभी लोकतंत्र का चेहरा उज्जवल होता है।”
उत्तराखंड की आत्मा अब भी जीवित है
भले ही राज्य स्थापना की 25 वर्ष की यात्रा में अनेक निराशाएँ मिलीं,
परंतु यह सत्य है कि उत्तराखंड की आत्मा अब भी जीवित है —
उस माँ में जो पहाड़ की गोद में अपने बेटे को विदा करती है,
उस सैनिक में जो सीमा पर तैनात है,
उस शिक्षक में जो दो घंटे पैदल चलकर गाँव के विद्यालय पहुँचता है,
और उस पत्रकार में जो बिना संसाधन जनता की आवाज़ बनता है।
“उत्तराखंड केवल भूगोल नहीं, भाव है;
यह केवल राज्य नहीं, संघर्ष की साधना है।”
रजत जयंती का यह वर्ष हमें याद दिलाता है कि
यदि आत्ममंथन ईमानदारी से किया जाए,
तो अगली स्वर्ण जयंती तक एक नया उत्तराखंड बन सकता है —
जहाँ विकास संवेदना से जुड़ा हो,
जहाँ राजनीति सेवा बने,
और जहाँ हर पहाड़ पुनः जीवन से भर उठे।
राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आत्ममंथन : “निष्कर्ष और लोकशक्ति का पुनर्जागरण”
निष्कर्ष और लोकशक्ति का पुनर्जागरण
रजत जयंती वर्ष, यानी 25 वर्षों का यह पड़ाव—सिर्फ़ एक सरकारी उत्सव नहीं, बल्कि जनता, मिट्टी, और इतिहास की आत्मा से जुड़ा हुआ वह क्षण है, जहाँ हमें ठहरकर यह प्रश्न पूछना चाहिए—क्या हमने वह राज्य बनाया, जिसका सपना हमारे शहीद आंदोलनकारियों ने देखा था? क्या वह उत्तराखंड वास्तव में जन्म ले पाया है, जो ‘पर्वतों की आत्मा और लोकजीवन की चेतना’ से संचालित होना चाहिए था?
आज जब राज्य स्थापना की रजत जयंती पर सरकारी भवनों में झंडे फहराए जा रहे हैं, मंचों पर भाषणों की गूंज है, तब गाँवों की ढलानों पर बैठे बुजुर्ग आज भी कहते हैं—“हमें सड़क नहीं, रोज़गार चाहिए; हमें नारे नहीं, हमारा बेटा घर लौटे इतना ही चाहिए।” यही संवाद दरअसल रजत जयंती के वास्तविक अर्थ की ओर संकेत करता है—राज्य नहीं, जन-राज्य चाहिए; शासन नहीं, लोकशक्ति चाहिए।
उत्तराखंड के भविष्य का पथ : आत्मबल और लोकनीति का संगम
राज्य की स्थापना की मूल भावना ‘लोक-भागीदारी’ पर आधारित थी। पर्वतीय समाज ने यह राज्य इसलिए मांगा था कि यहाँ की नीति, यहाँ के भूगोल, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जनजीवन के अनुसार बने। परंतु दुर्भाग्य यह है कि 25 वर्षों में नीति निर्माण की दिशा फिर से मैदानी मापदंडों के अधीन होती चली गई।
भविष्य का उत्तराखंड तभी समृद्ध हो सकता है जब नीति निर्माण में स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक कृषि प्रणाली, और सामुदायिक प्रशासन मॉडल को प्राथमिकता दी जाए। गाँवों में ग्रामसभा की भूमिका केवल दस्तावेज़ी औपचारिकता नहीं, बल्कि निर्णय का आधार बने।
“लोकनीति तभी फलती है जब नीति की जड़ें लोक में हों।”
—यह वाक्य हमें याद रखना होगा।
राज्य के भविष्य का निर्माण केवल योजनाओं या घोषणाओं से नहीं, बल्कि ‘नव-विश्वास’ से होगा—वह विश्वास जो युवा पीढ़ी को अपनी मिट्टी से जोड़ता है। स्कूलों में “मेरा गाँव–मेरा गौरव” जैसी स्थानीय विषयवस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम अनिवार्य किए जाने चाहिए।
आर्थिक दिशा : आत्मनिर्भर पर्वतीय अर्थव्यवस्था
उत्तराखंड का भविष्य आत्मनिर्भरता पर निर्भर है। राज्य की प्राकृतिक पूंजी (जल, जंगल, जमीन) का उपयोग अब ‘रॉयल्टी’ के बजाय ‘स्वामित्व’ के मॉडल पर आधारित होना चाहिए।
गाँवों में पलायन को रोकने के लिए छोटे कृषि–औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने होंगे। स्थानीय उत्पाद जैसे—रसीला माल्टा, झंगोरा, गहत, मंडुवा, सिलाई, जड़ी-बूटियाँ—के लिए “हिमालयी ब्रांड” का निर्माण हो। इससे न केवल स्थानीय रोजगार सृजित होगा, बल्कि युवाओं को अपनी मिट्टी से जुड़ने का भाव भी मिलेगा।
आज राज्य को चाहिए “ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी”, जो पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देती हो। नदियों के किनारे कंक्रीट नहीं, कुमायूं–गढ़वाल की पारंपरिक जलसंरचना पुनर्जीवित हो।
कृषि विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को चाहिए कि वे “लघु किसान अनुसंधान केंद्र” स्थापित करें, जहाँ खेत से जुड़ी समस्याओं पर तत्काल समाधान हो सके।
सांस्कृतिक पुनर्जागरण : लोकगीतों में छिपी विकास की चेतना
राज्य निर्माण का आधार केवल भौगोलिक नहीं था, यह सांस्कृतिक चेतना का भी आंदोलन था। आंदोलन के दिनों में जब ‘बदरी के धाम, हमारा उत्तराखंड महान’ के नारे गूंजते थे, तब हर गीत, हर झोला, हर ढोल-दमाऊ एक संदेश देता था—यह भूमि केवल संसाधन नहीं, संस्कार है।
आज आवश्यकता है कि हम उत्तराखंड की लोकसंस्कृति को विकास के साथ जोड़ें।
विद्यालयों में गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाए।
सांस्कृतिक विभाग केवल उत्सव न मनाए, बल्कि लोकसंस्कृति संरक्षण मिशन चलाए।
पारंपरिक संगीत, नृत्य, लोककथाओं को डिजिटाइज कर युवाओं तक पहुँचाया जाए।
पहाड़ी वस्त्र, भोजन और कला को ‘हेरिटेज इकोनॉमी’ का हिस्सा बनाया जाए।
क्योंकि कोई भी समाज तब तक जीवित नहीं रह सकता, जब तक उसकी भाषा जीवित है।
नीति-सुधार : नौकरशाही नहीं, उत्तरदायी शासन चाहिए
राज्य निर्माण आंदोलन के दिनों में नारा था—“हमारा राज, हमारे गाँव का राज।” पर आज भी नीति-निर्माण देहरादून के वातानुकूलित दफ्तरों में होता है। निर्णयों में न जनता की भागीदारी है, न पंचायतों की राय।
अब समय है कि राज्य “पर्वतीय नीति आयोग” बनाए, जिसमें समाजशास्त्री, आंदोलनकारी, पर्यावरणविद् और किसान शामिल हों।
राज्य में “जन-सुनवाई आयोग” को संवैधानिक दर्जा मिले ताकि जनहित से जुड़ी शिकायतें सीधे शासन स्तर तक पहुँचे।
शासन-प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु प्रत्येक विभाग की वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन सार्वजनिक की जाए, और जनता की समीक्षा अनिवार्य हो।
जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का नारा तभी सार्थक होगा जब जन-जवाबदेही अधिनियम लाया जाए।
उत्तराखंड का जनमानस और लोकशक्ति का पुनर्जागरण
“लोकशक्ति” कोई काल्पनिक शब्द नहीं, यह वही शक्ति है जिसने आंदोलन के दिनों में जेलें भरीं, सड़कों पर संघर्ष किया, और पर्वतों की धूल में अपना खून मिलाया। आज वही लोकशक्ति निराशा में है—क्योंकि सत्ता ने उसे हाशिए पर डाल दिया।
अब आवश्यकता है “लोकशक्ति पुनर्जागरण आंदोलन” की—जहाँ जनता अपने अधिकारों के लिए फिर से सजग हो।
ग्राम स्तर पर लोकसंवाद मंडल बने जो नीतियों की समीक्षा करें।
युवाओं के लिए “राज्य निर्माण कैम्प” आयोजित हों, जहाँ उन्हें आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाए।
मीडिया को भी चाहिए कि वह सरकार की घोषणाओं से अधिक जनता की आवाज़ बने।
यह पुनर्जागरण केवल राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक पुनर्जागरण भी होगा—जहाँ उत्तराखंड के नागरिक अपने अंदर की चेतना को पहचानेंगे।
महाकवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था—
“जो बीत गई सो बात गई,
जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था।”
परंतु उत्तराखंड को बीते हुए गौरव पर नहीं, आने वाले भविष्य पर विश्वास करना होगा।
निष्कर्ष : “वन्दे मातरम्” की भावना में नव-उत्तराखंड
राज्य निर्माण का अर्थ केवल नई सीमाओं का खींचना नहीं, बल्कि नई चेतना का अंकुरण है।
वर्तमान में जब देशभर में “वन्दे मातरम्” के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब उत्तराखंड को भी इस राष्ट्रगीत की भावना से सीख लेनी चाहिए—कि मातृभूमि की सेवा केवल भावनाओं से नहीं, कर्म से होती है।
उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष हमें यह सिखाता है कि यह राज्य अभी अधूरा है—जब तक हर गाँव में रोजगार नहीं, हर बच्चे को शिक्षा नहीं, हर महिला को सुरक्षा नहीं, और हर किसान को सम्मान नहीं।
यही वह क्षण है जब हमें पुनः कहना होगा—
“हम राज्य नहीं, लोक-राज चाहते हैं।”
“हम विकास नहीं, संवेदनशीलता चाहते हैं।”
“हम सरकार नहीं, अपने अस्तित्व का सम्मान चाहते हैं।”
यदि यह भाव जन-जन के भीतर पुनः जाग्रत हुआ, तो यह रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड के स्वर्ण भविष्य का आधार बनेगा।
वर्ना यह भी एक और सरकारी उत्सव बनकर रह जाएगा—जिसे कुछ ने मनाया और बहुतों ने भुला दिया।
डिस्क्लेमर (Disclaimer):
यह सम्पादकीय लेख ‘सरहद का साक्षी’ के सम्पादक केदार सिंह चौहान ‘प्रवर’ द्वारा राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर लिखित विचारात्मक, विश्लेषणात्मक व साहित्यिक प्रस्तुति है। लेख का उद्देश्य राज्य निर्माण के मूल सिद्धांतों, लोकशक्ति की भूमिका तथा नीति-सुधार की आवश्यकता पर विमर्श प्रस्तुत करना है, न कि किसी व्यक्ति या संस्था की आलोचना करना। लेख का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर जनचेतना, नीति विमर्श और सांस्कृतिक पुनर्विचार को प्रोत्साहित करना है।
(केदार सिंह चौहान ‘प्रवर’)